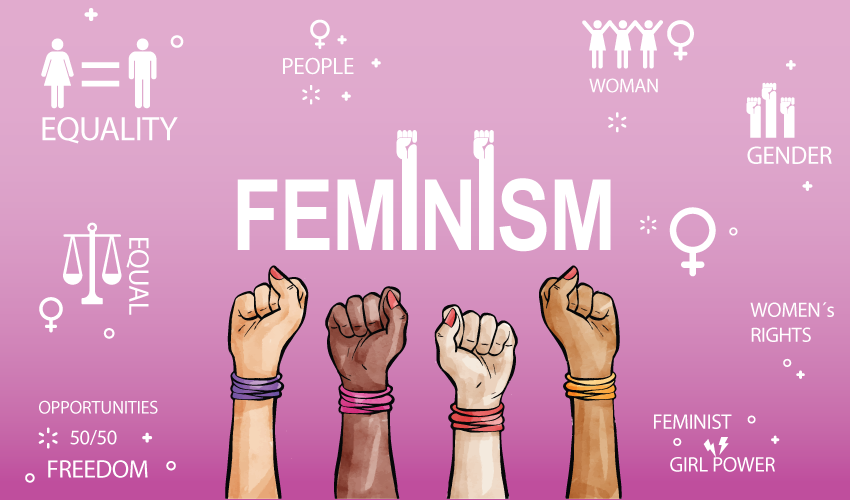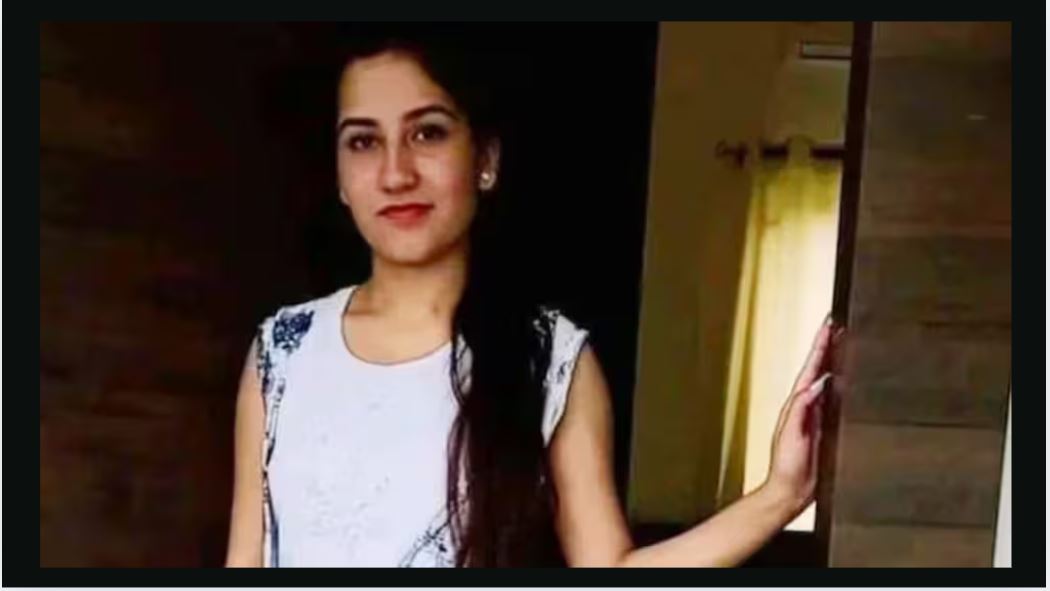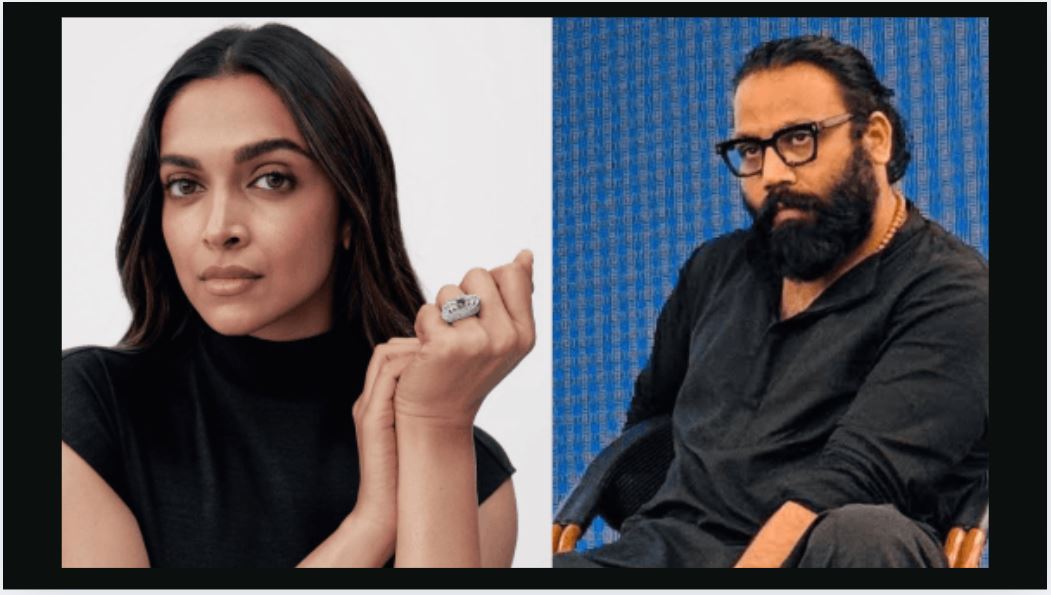अक्सर आप सुनते ही होंगे कि ये फेमेनिस्ट जहां देखो अपना झंडा लेकर चल देती हैं। घर तोड़ना, महिलाओं को भड़काना और उन्हें बहकाना इनका काम है। ताने कई बार ऐसे भी मिलते हैं कि औरतों को काम से बचना हो तो फेमिनिज्म का हथियार मिल जाता है। इन्हें ऐसे तो फेमिनिज्म सुझता है, लेकिन जहां कोटे या सीट की बात आती है, इन्हें वहां रिजर्वेशन चाहिए, वगैरह…वगैरह…
कई लोगों को तो आज भी फेमिनिज्म के मतलब से मतलब नहीं है, उन्हें बस इसे एक गाली की तरह उन औरतों पर इस्तेमाल करना है, जो चुप–चाप सब कुछ झेलने में नहीं बल्कि मुंह खोलकर अपने अधिकार मांगने में विश्वास रखती हैं। दरअसल, आज भी लोग झूठी मार्डन सोच का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात आती है, तो वहां अपने कदम पीछे खींच लेते हैं।
सही मायनों में सालों से चले आ रहे फेमिनिज्म यानी नारीवादी आंदोलन का असली मतलब बराबरी है। समाज में मर्द और औरत के अधिकारों, कामों और जिम्मेदारियों के बीच बराबरी। फेमेनिस्ट सिर्फ औरत ही नहीं कोई मर्द भी हो सकता है अगर वो जेंडर समानता की वकालत करता है तो। रही बात रिजर्वेशन की तो वो सालों से पीछे चल रही महिलाओं को बराबरी तक लाने का एक रास्ता है। उनकी समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका।
जन्म से ही लड़के–लड़की के बीच भेद
पितृसत्ता के इस समाज में जन्म से ही लड़के–लड़की के बीच भेद का बीज बो दिया जाता है। लड़का घर के काम नहीं करेगा, लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी। लड़का शर्ट–पैंट पहनेगा तो लड़की स्कर्ट, फ्रॉक या सूट पहनेगी। ये भेद भी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। लड़की शादी के बाद दूसरे घर जाएगी, तो वहीं लड़का अपने ही घर में दूसरे घर से आई अपनी बीवी पर एहसान दिखाएगा कि तुम्हारे लिए कमाता हूं। बस फिर यही भेद की खाई गहरी होती जाती है और महिलाओं को दबाने का अधिकार पुरुषों को जन्म से ही मिल जाता है।
हालांकि अब ये तस्वीर बदल रही है। लड़कियां पढ़–लिख कर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बदलाव बहुत धीमा है। लड़की अगर शिक्षित और नौकरी वाली है फिर भी उसे समाज और घरवालों के तमाम दबावों के बीच घुट–घुट कर जीने को ही मजबूर होना पड़ता है। जो लड़कियां इस बात को नहीं मानती उन्हें फेमेनिस्ट का टैग एक गाली की तरह चिपका दिया जाता है। इसमें कोई दो राह नहीं कि समाज जिस बात का विरोध करता है हम उस बात के विरोध में खड़े होते ही फेमिनिस्ट बना दिये जाते हैं या फ़ेमिनिस्ट बन जाते हैं।
पितृसत्ता की समस्या का समाधान मातृसत्ता नहीं
जानी–मानी नारीवादी कमला भसीन कहती थी कि हमारे समाज में कई महिलाएं हैं, तो पितृसत्ता को पोसती हैं, तो वहीं कई पुरुष भी हैं, तो महिला अधिकारों के लिए मुखर हैं। उनके अनुसार पितृसत्ता की समस्या का समाधान कभी भी मातृसत्ता नहीं हो सकती क्योंकि बात यहां बराबरी की है। सत्ता परिवर्तन की नहीं। किसी का किसी पर आधिपत्य या दबाव एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बहरहाल, ये शब्द बराबारी सुनने में भले ही बड़ा न लगता हो, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं और यहीं कारण है कि ये रूढ़िवादियों को चुभते हैं। ज़रा सोचिए, अगर लड़कियां बचपन से लड़कों के बराबर हक़ मांगने लगें, ब्याह के बाद अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाने से मना कर दें। शादी के बाद घर संभालने और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से पीछे हट जाएं तो पितृसत्ता की जड़े हिल जाएंगी। घरों में बैठकर आराम से हुकुम चलाने वाले मर्दों की सत्ता छिन जाएगी और यही कारण है कि मर्द सबसे ज्यादा इस पितृसत्ता के पैरोकार माने जाते हैं। उन्हें नारीवाद से नफरत है क्योंकि ये उनकी सत्ता को सीधे–सीधे चुनौती है।
Image credit-Team Attorneylex